Join Us Now!
Applyभारतीय संविधान के अनुच्छेद 12
अनुच्छेद 12 के अनुसार, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल..
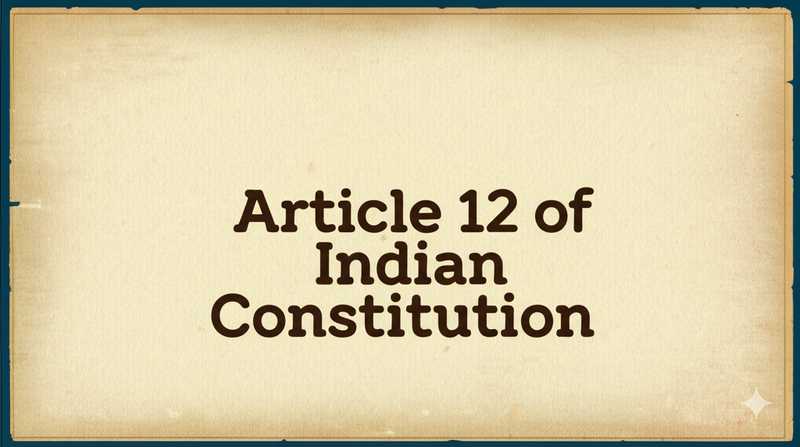
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में "राज्य" शब्द की परिभाषा क्या है? इसको विस्तार से समझाइये।🔗
अनुच्छेद 12 के अनुसार, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:
-
भारत सरकार और संसद (Government and Parliament of India): इसका अर्थ है केंद्र की कार्यपालिका (Executive) और विधायिका (Legislature)।
- कार्यपालिका (Executive): राष्ट्रपति (President), उपराष्ट्रपति (Vice-President), प्रधानमंत्री (Prime Minister), मंत्रिपरिषद (Council of Ministers), और भारत सरकार के विभिन्न विभाग और एजेंसियां (जैसे आयकर विभाग)।
- विधायिका (Legislature): संसद (Parliament), जिसमें लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) शामिल हैं।
-
प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल (Government and Legislature of each State): इसका अर्थ है राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका।
- कार्यपालिका (Executive): राज्यपाल (Governor), मुख्यमंत्री (Chief Minister), राज्य मंत्रिपरिषद (State Council of Ministers), और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग।
- विधायिका (Legislature): राज्य विधानमंडल (State Legislature), जिसमें विधानसभा (Legislative Assembly) और कुछ राज्यों में विधान परिषद (Legislative Council) भी शामिल है।
-
भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी (All local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India):
- स्थानीय प्राधिकारी (Local Authorities): इसका अर्थ है नगरपालिकाएं (Municipalities), जिला बोर्ड (District Boards), पंचायतें (Panchayats), इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (Improvement Trusts), पोर्ट ट्रस्ट (Port Trusts) आदि। ये संस्थाएं स्थानीय स्वशासन (local self-government) से संबंधित कार्य करती हैं। उदहारण (Example): दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi), बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation)
- अन्य प्राधिकारी (Other Authorities): यह एक व्यापक (wide) शब्द है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विभिन्न मामलों में की है। इसमें वे सभी निकाय (bodies) शामिल हैं जो या तो सांविधिक (statutory - कानून द्वारा निर्मित) हैं या गैर-सांविधिक (non-statutory), और जो सरकार के कार्यों (functions) को पूरा करते हैं या सरकार द्वारा नियंत्रित (control) होते हैं।
- सांविधिक निकाय (Statutory Bodies): भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India - LIC), तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (Oil and Natural Gas Commission - ONGC), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission)।
- गैर-सांविधिक निकाय (Non-Statutory Bodies): भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India - BCCI) (कुछ मामलों में), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research - CSIR)।
"अन्य प्राधिकारी" (Other Authorities) शब्द की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट का क्या दृष्टिकोण रहा है? महत्वपूर्ण केस लॉ (Case Laws) का वर्णन करें।🔗
"अन्य प्राधिकारी" शब्द की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर विभिन्न मामलों में की है। यहां कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ दिए गए हैं:
-
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मोहन लाल (Rajasthan State Electricity Board vs. Mohan Lal), 1967: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अन्य प्राधिकारी" शब्द में वे सभी निकाय शामिल हैं जिन्हें कानून द्वारा शक्तियां (powers) दी गई हैं, भले ही वे वाणिज्यिक (commercial) कार्य कर रहे हों।
-
सुखदेव सिंह बनाम भगतराम (Sukhdev Singh vs. Bhagatram), 1975: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि LIC, ONGC और IFC जैसी सांविधिक निगम (statutory corporations) "राज्य" हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य (public functions) करते हैं।
-
रमणा दयाराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (Ramana Dayaram Shetty vs. International Airport Authority), 1979: इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए मानदंड (criteria) निर्धारित किए कि क्या कोई निकाय "राज्य" का साधन (instrumentality) है।
- क्या निकाय (body) की संपूर्ण शेयर पूंजी (entire share capital) सरकार के पास है?
- क्या निकाय का खर्च (expenditure) सरकार उठाती है?
- क्या निकाय को सरकार द्वारा एकाधिकार (monopoly) का दर्जा दिया गया है?
- क्या निकाय पर सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण (deep and pervasive control) है?
- क्या निकाय सार्वजनिक महत्व (public importance) के कार्य करता है?
- क्या सरकार का कोई विभाग (department) निगम को हस्तांतरित (transfer) किया गया है?
-
अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब (Ajay Hasia vs. Khalid Mujib), 1981: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक सोसायटी (society), जो एक कॉलेज का संचालन करती थी और सरकार द्वारा नियंत्रित थी, "राज्य" थी।
-
प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी (Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology), 2002: सुप्रीम कोर्ट ने माना की CSIR, जो की एक सोसाइटी है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, आर्टिकल 12 के तहत 'अन्य अथॉरिटी' है.
-
ज़ी टेलीफिल्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (Zee Telefilms vs. Union of India), 2005: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BCCI "राज्य" नहीं है क्योंकि यह सरकार द्वारा वित्तपोषित (funded) या नियंत्रित (controlled) नहीं है।
-
रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra), 2002: सुप्रीम कोर्ट ने ये माना की न्यायिक प्रक्रिया (judicial proceedings) को कभी भी मौलिक अधिकारो (fundamental rights) का उलंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता, और उच्चतर न्यायालय अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य या अन्य प्राधिकारियों के दायरे में नहीं आती हैं।
क्या न्यायपालिका (Judiciary) "राज्य" की परिभाषा के अंतर्गत आती है?🔗
यह एक जटिल प्रश्न है। अनुच्छेद 12 न्यायपालिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है।
-
न्यायिक कार्य (Judicial Functions): जब न्यायालय न्यायिक कार्य (जैसे मुकदमों का फैसला करना) करते हैं, तो आमतौर पर उन्हें "राज्य" नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और संविधान की रक्षा करते हैं।
-
प्रशासनिक कार्य (Administrative Functions): जब न्यायालय प्रशासनिक कार्य (जैसे नियम बनाना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना) करते हैं, तो उन्हें "राज्य" माना जा सकता है।
-
प्रेम गर्ग बनाम एक्साइज कमिश्नर एच.पी. (Prem Garg v. Excise Commissioner H.P.): सुप्रीम कोर्ट ने माना की जब न्यायपालिका की रूल-मेकिंग (rule making) शक्ति का सवाल उठता है तो वो 'राज्य' है।
इसलिए, न्यायपालिका को "राज्य" माना जाएगा या नहीं, यह उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति (nature) पर निर्भर करता है।
अनुच्छेद 12 का महत्व (Significance) क्या है?🔗
अनुच्छेद 12 का महत्व निम्नलिखित है:
-
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा (Protection of Fundamental Rights): यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार केवल सरकार के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उन सभी निकायों के खिलाफ भी लागू हों जो सरकार के कार्यों को करते हैं या सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं।
-
जवाबदेही (Accountability): यह "राज्य" की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सभी निकायों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाता है।
-
कानून का शासन (Rule of Law): यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी संस्था या व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
-
सुशासन (Good Governance): यह सुनिश्चित करता है की सभी पब्लिक अथॉरिटीज (public authorities) संविधान के नियमो और नैतिक आचरण का पालन करे.
Subscribe to our Website!
Get the latest updates, exclusive content and special offers delivered directly to your mailbox. Subscribe now!